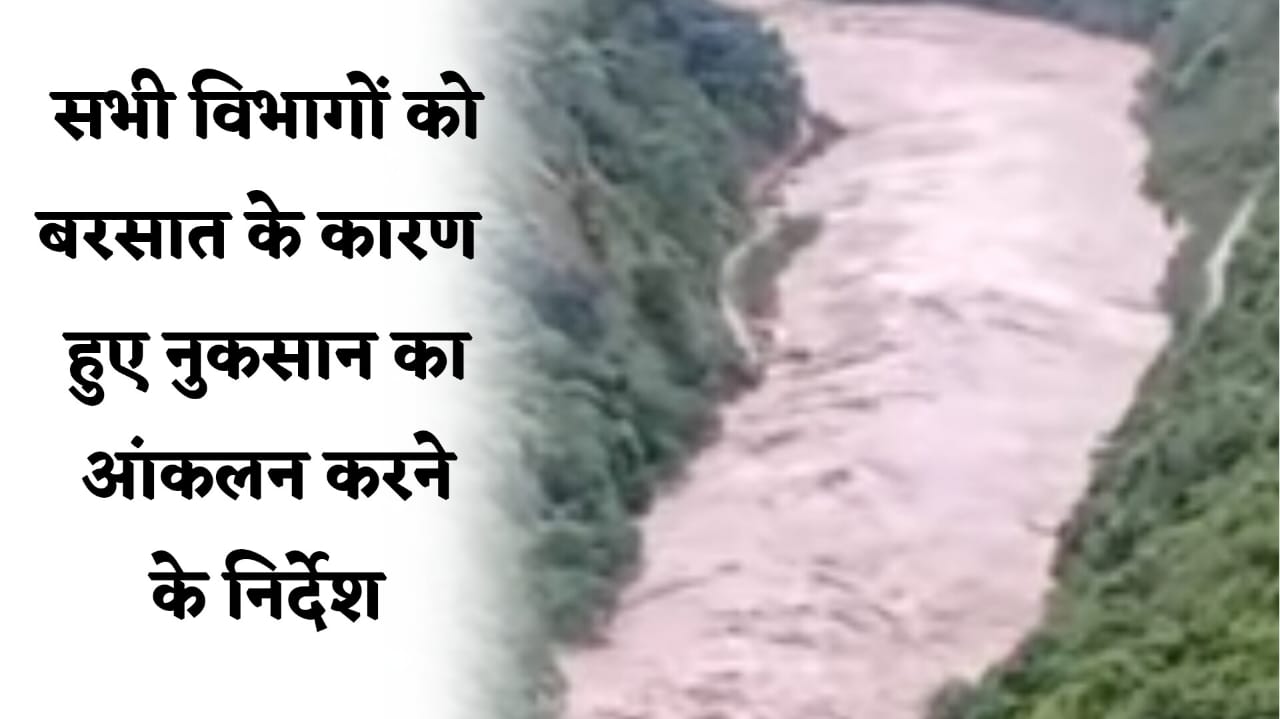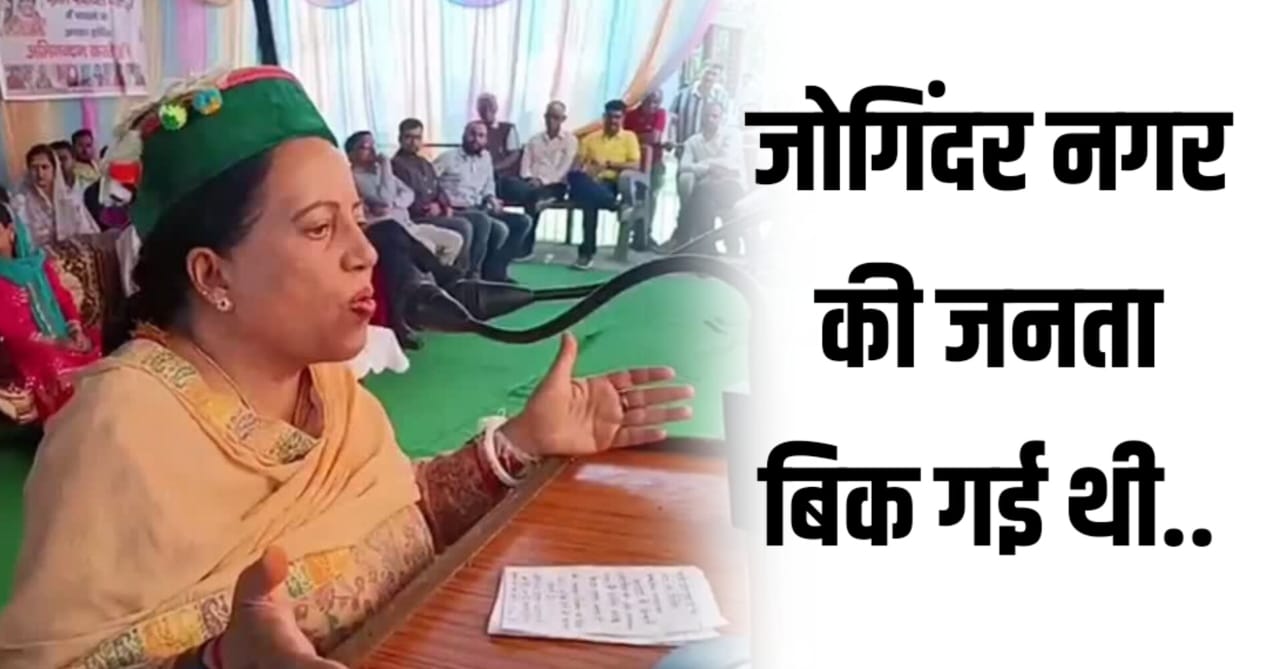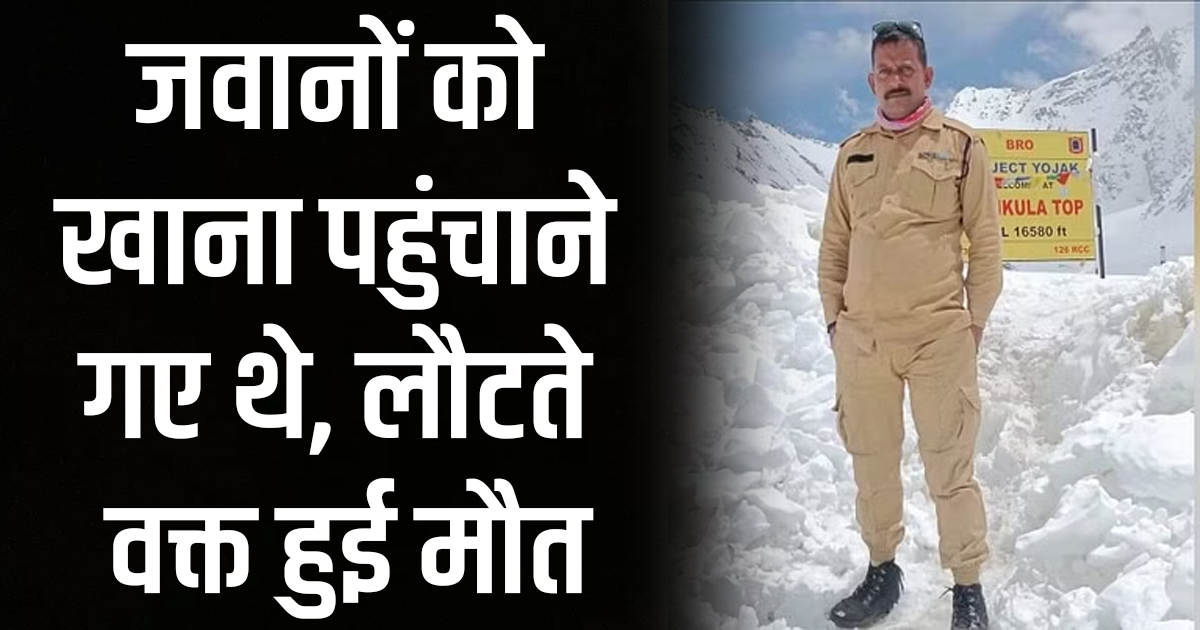जोगिंदरनगर: Dream 11 में चमकी किस्मत, कस पंचायत के संजीव कुमार ने जीते 40 लाख रुपये
जोगिंदरनगर: उपमंडल की कस पंचायत के एक व्यक्ति का फैंटेसी स्पोर्ट्स एप ड्रीम 11 (Dream 11) पर जैकपॉट लगा है। कस पंचायत के संजीव कुमार ने ड्रीम 11 में 40 लाख रुपये जीते हैं। संजीव कुमार ने बताया कि उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। 10-12 गाड़ियां उनके पास है। कारोबार के लिए उन्होंने बैंकों से … Read more